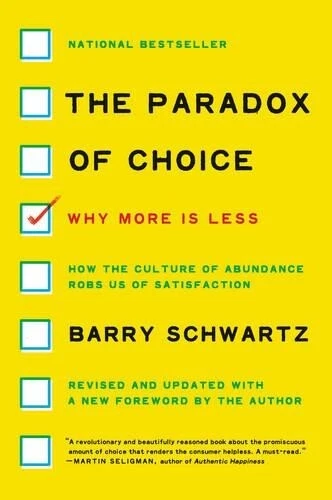THE PARADOX OF CHOICE - Why More is Less
Barry Schwartz
इंट्रोडक्शन
आज से 10 साल पहले जींस खरीदना आसान था। आप दुकान में जाते थे, स्टॉफ को अपना साइज़ बताते थे और आपका काम हो जाता था। इस चीज़ में आधे घंटे से भी कम समय लगता था।
लेकिन आज यही काम कितना मुश्किल हो गया है। दुकानदार आपसे सिर्फ़ आपका साइज़ ही नहीं पूछता है बल्कि ये भी पूछता है की आपको जींस स्लिम-फिट चाहिए या रिलैक्स्ड, बैगी चाहिए या स्किनी। यहाँ पर भी उसके सवालों की बौछार थमती नहीं है, वह ये भी पूछता है की जींस फेडेड होनी चाहिए या रेगुलर या फटी हुए डिजाइन होनी चाहिए?
सिर्फ़ जींस में ही बहुत सारे ऑप्शन नहीं हैं। यह आपकी लाइफ के अलग-अलग एरिया में भी मौजूद है, जैसे की: आपको कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, किस चीज़ में अपना करियर बनाना चाहिए और कैसा रिश्ता बनाना चाहिए।
दूसरी चॉइस का होना अच्छी बात है। यह हमें याद दिलाता है की हमारा हमारी ज़िंदगी पर कंट्रोल है और हम आज़ाद हैं। पर बहुत सारे ऑप्शन के होने से बुरा असर भी पड़ सकता है। इस वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस, यहां तक की क्लिनिकल डिप्रेशन भी हो सकता है।
इस समरी में, आप जानेंगे की कैसे ज़्यादा चॉइस का होना सिर दर्द बन सकता है। आप यह भी जानेंगे की कम चॉइस रखना अच्छा क्यों होता है। आखिर में, आप सीखेंगे की अपने फैसले से खुश रहने के लिए आपको ढेर सारे ऑप्शन को कैसे हैंडल करना चाहिए।
Let’s Go Shopping
इस बुक के ऑथर बैरी श्वार्ट्ज, हाल ही में राशन का समान खरीदने गए थे। उन्हें क्रैकर्स खाने का मन कर रहा था तो बैरी उस तरफ़ गए जहां क्रैकर्स रखे हुए थे। जब उन्होंने देखा की वहां 50 से भी ज़्यादा क्रैकर्स की वैरायटी है तो वह हैरान हो गए। कुछ ब्रैंड अपने क्रैकर्स में कम नमक होने का दावा कर रहे थे तो दूसरे ब्रैंड का दावा था की उनके क्रैकर्स में फैट नहीं है। कुछ बेहद छोटे साइज़ के थे तो कुछ एवरेज साइज़ के।
लेकिन वहाँ ढेर सारे ऑप्शन सिर्फ़ क्रैकर्स में ही नहीं थे। उन्होंने इस चीज़ को कुकीज़, जूस और चिप्स में भी नोटिस किया। यही चीज़ उन्होंने दवाई, शैंपू, साबुन और डेंटल फ्लॉस में भी देखा।
आमतौर पर एक सुपरमार्केट में 30,000 से भी ज़्यादा आइटम होते हैं। ऊपर से, हर साल कम से कम 20,000 नए प्रोडक्ट को add किया जाता है।
अगर किसी एक ब्रैंड का क्रैकर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप दूसरा ब्रैंड ट्राई कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ अलग-अलग तरह के ऑप्शन में से चुनना ही इकलौती उलझन नहीं होती है जिसका सामना हमें करना पड़ता है। हमें हमारे राशन के सामान के दाम को भी ध्यान में रखना होता है। जो सामान आप ले रहे हैं क्या वो उस दाम के लायक है? क्या उसका स्वाद अच्छा है या क्या उसमें सोडियम और फैट कम है?
हो सकता है की आप राशन का सामान लेते वक्त कार्बोहाइड्रेट्स का परसेंटेज या कैलरीज़ के बारे में चिंता नहीं करते होंगे पर फिर भी ढेर सारे ऑप्शन होने की वजह से आपकी ज़िंदगी के दूसरे कई पहलू पर असर पड़ सकता है। इसके कुछ example हैं गैजेट और अप्लायंसेज। कुकी का बॉक्स खरीदने के मुकाबले में एक फ़ोन खरीदते समय हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है।
फ़ोन महंगे होते हैं इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है की वह लंबे समय तक चले और अपने दाम के लायक हो। पर गैजेट के एक स्टैंडर्ड दुकान में सिर्फ़ एक ब्रैंड या एक मॉडल का फोन नहीं बेचा जाता है। वहां दर्ज़नों ब्रैंड और मॉडल होते हैं जिनमें से हमें चुनना पड़ता है। अब यहां पर चुनना मुश्किल हो जाता है।
दूसरी मुश्किल चॉइस है यह चुनना की आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं। एजुकेशन लोगों को स्किल सिखाने में और सोसायटी में मददगार बनाने में मदद करती है। पहले एक जैसी डिग्री पूरी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट सेम हुआ करते थे पर अब ऐसे इंस्टीट्यूशन आ गए हैं जहां स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट खुद चुनते हैं।
वह प्रोफेसर के लेक्चर में बैठते हैं लेकिन अगर उन्हें उस डिस्कशन में मज़ा नहीं आता है तो वे वहां से निकल जाते हैं। फिर, वो स्टूडेंट्स दूसरे क्लास में जाकर देखते हैं की उन्हें वहां पढाया जाने वाला सब्जेक्ट या टॉपिक पसंद आ रहा है या नहीं।
स्ट्डीज से पता चला है की लोग अब शॉपिंग करने में ज़्यादा समय बिताते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि अब चॉइसेस ही इतने बढ़ चुके हैं। लेकिन इन स्ट्डीज से यह भी पता चला है की भले ही लोग शॉपिंग करने में ज़्यादा समय बिता रहे हैं पर वे इसे पहले से कम एंजॉय करने लगे हैं।
मामला बड़ा उलझा हुआ सा लग रहा है ना? किसे नहीं पसंद आएगा की उसके पास चुनने के लिए ढेर सारे ऑप्शन हों और अगर आप ढेर सारे ऑप्शन में से नहीं चुनना चाहते हैं तो आप आराम से उसे चुन सकते हैं जिसे आप हमेशा से पसंद करते आए हैं। लेकिन ये बात नहीं है। इसका सबूत स्ट्डीज की एक सीरीज़ में है जिसे “व्हेन चॉइस इज़ डिमोटिवेटिंग” के नाम से जाना जाता है।
इन स्ट्डीज के रिसर्चर्स सही अनुमान लगाते थे। उन्होंने बताया की ज़्यादा ऑप्शन होना असल में हमें परेशान और निराश कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे फैसला करने में ज़्यादा मेहनत लगती है। ज़्यादा मेहनत का लगना असल में कुछ लोगों को कुछ भी खरीदने से रोक देता है।
लेकिन अगर वो कुछ खरीदते भी हैं तो उसे पसंद करने में लगने वाली मेहनत की वजह से इतने परेशान हो जाते हैं की शॉपिंग को एंजॉय नहीं कर पाते।
कई ऑप्शन होने से संतुष्ट ना हो पाने की दूसरी वजह है बार-बार दूसरे ऑप्शन का पसंद आना। जैसे, मान लीजिए कि लीज़ा एक घंटे तक सोचने के बाद किसी ब्रैंड के परफ्यूम को खरीदने का फैसला करती है, लेकिन जब आखिर में वह उसे खरीद लेती है तो उसे खुशी महसूस नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह ये सोचती रहती है की शायद वो दूसरा परफ्यूम चुन सकती थी।
इसलिए, बहुत सारे ऑप्शन का होना असल में अच्छी चीज़ नहीं है। यह परेशानी का कारण ज़्यादा बन जाती है। इसे ही ‘पैराडॉक्स ऑफ़ चॉइस’ कहा जाता है।
Deciding and Choosing
कोई चीज़ choose करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर तब जब सारे ऑप्शन अच्छे होते हैं। जैसे, मान लीजिए कि जेरेमी नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने का प्लान बना रहा है। इसके लिए उसे हर ऑप्शन के प्राइस, लोकेशन, सेफ्टी और कंडीशन को ध्यान में रखना होगा और यहीं से जेरेमी की परेशानी शुरू होती है। जैसा घर उसे चाहिए था उस बजट में, लोकेशन पर और कंडीशन में कुछ अपार्टमेंट्स उसे पसंद आते हैं। जेरेमी यह भी देखता है की उनमें से सभी अपार्टमेंट बिलकुल सेफ हैं। अब उसे कौन सा अपार्टमेंट चुनना चाहिए? उसे कौन से फीचर को प्रायोरिटी देनी चाहिए? क्या जेरेमी को शहर के पास रहने के लिए महंगी जगह को चुनना चाहिए?
सही डिजिशन लेने में आमतौर पर आपके गोल्स शामिल होते हैं। आपको तय करना होगा की हर गोल आपके लिए कितना ज़रूरी है।
अगला, आपको अपने ऑप्शंस पर ध्यान देना होगा। आखिर में, सभी ऑप्शंस को evaluate करें और उनमें से उस ऑप्शन को चुनें जो आपके गोल्स को पूरा करने का ज़्यादा चांस रखता हो।
जेरेमी का गोल था रेंट पर एक अच्छा अपार्टमेंट लेना। जब टाउन में अपार्टमेंट लेने की बात आती है तो उसके पास कई ऑप्शन थे। उसने हर अपार्टमेंट को अपनी डेफिनिशन के हिसाब से चेक किया कि अच्छा अपार्टमेंट कैसा होना चाहिए। उसने तय किया की अच्छा अपार्टमेंट वह होगा जो नया बना हो और मॉल और ट्रेन स्टेशन के नज़दीक हो।
असल में, अपने गोल्स को तय करना बहुत मुश्किल हो सकता है। आपका प्लान होता है खुद से यह जरूर पूछना की, “आप क्या चाहते हैं?” हालांकि, आप क्या चाहते हैं यह पता होने का मतलब है पहले से यह सोचकर रखना की आपकी चॉइस की वजह से आपको कैसा महसूस होगा। यह करना कोई आसान चीज़ नहीं है।
हम क्या चाहते हैं इसे तय करना मुश्किल क्यों है इसके कई अलग-अलग वजहों में से एक है “पीक-एंड” रूल। इस बारे में साइकोलॉजिस्ट और नोबल प्राइज़ विनर डैनियल कहनेमान ने बताया है। कोई एक्सपीरियंस कितना अच्छा है इसे “पीक-एंड” रूल में दो चीजों के हिसाब से तय किया जाता है जो है: जब वह एक्सपीरियंस अपने पीक पर था तो आपको कैसा महसूस हुआ था और जब वह एक्सपीरियंस खत्म हो गया था तब आपको कैसा महसूस हुआ था।
आइए इसे एक example से समझते हैं। मान लीजिए आपने अक्टूबर में दो बार वेकेशन पर जाने का प्लान बनाया।
पहली बार छुट्टी सिर्फ़ एक हफ्ते की थी। भले ही वह कम समय की थी पर आपने बीच पर स्विमिंग करना और नए फ्रेंड्स बनाना बहुत एंजॉय किया। इस खुशी में आपकी छुट्टियां कब खत्म हो गई आपको पता ही नहीं चला।
दूसरी बार छुट्टी तीन हफ्तों की थी। यह आपकी पहली छुट्टी के मुकाबले ज़्यादा लंबे समय के लिए थी। इसमें भी आपको मज़ा आया। हालांकि, आखिर के कुछ दिनों में ये छुट्टी बहुत बोरिंग हो गई थी।
आप सोचेंगे की दूसरी छुट्टी के मुकाबले में पहली छुट्टी ज़्यादा अच्छी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा माइंड किसी एक्सपीरियंस की इंटेंसिटी पर ध्यान देता है। पहली छुट्टी में आपको ज़्यादा मजा आया था इसलिए आप सोचेंगे की वह ज़्यादा अच्छा वेकेशन था, लेकिन यह सच नहीं है। दूसरे वेकेशन में आपको ज़्यादा समय तक रिलैक्स करने मिला था। आपका माइंड इसे मानने से इंकार कर देता है क्योंकि वो किसी एक्सपीरियंस की इंटेंसिटी को प्रायोरिटी देता है।
तो, अगर आपके माइंड में भेद-भाव है तो आप क्या कर सकते हैं? क्या इससे बाहर निकलने का कोई तरीका है? हां, बिलकुल है और ऐसा आप अपने गोल्स को clearly सेट करके कर सकते हैं।
When Only the Best Will Do
सही चीज़ को चुनने में आपके गोल्स और वैल्यूज़ शामिल होते हैं।
मैक्सिमाइज़र उस इंसान को कहा जाता है जिसका गोल होता है सबसे बेस्ट चीज़ चुनना। सेटिस्फाइसर वह इंसान होता है जो ऐसी चीज़ों को भी चुन लेता है जो उसे थोड़ी सी भी अच्छी लगती है।
जैसे, मान लीजिए कि वॉल्टर एक मैक्सिमाइज़र हैं। जब वह कोई नया स्वेटर खरीदने का फैसला करते हैं तो वह जानना चाहते हैं की कौन सा स्वेटर सबसे बेस्ट है। वॉल्टर अपने फेवरेट दुकान में जाते हैं और उन्हें एक क्यूट सा स्वेटर मिलता है जो उन्हें पसंद आ जाता है। वह उनके बजट में था, उन्हें बहुत अच्छे से फिट आ रहा था और उसका कपड़ा भी बहुत अच्छा था।
पर क्योंकि वॉल्टर एक मैक्सिमाइज़र है इसलिए वह उस क्यूट से स्वेटर को नहीं खरीदते। इसके बजाय, वह दूसरे दुकान में जाते हैं और दूसरे स्वेटर को ट्राई करते हैं। एक मैक्सिमाइजर को अपने आपको विश्वास दिलाना पड़ता है की उनकी खरीदी हुई हर चीज़ सबसे बेस्ट और अच्छी है इसलिए वह एक के बाद एक दुकान में जाने में समय बर्बाद कर देते हैं। अगर आपको बहुत सारे ऑप्शन में से चुनना पड़े तो इससे थकान और निराशा भी हो सकती है।
बेशक, सभी ऑप्शन को टेस्ट करना मुमकिन नहीं है पर मैक्सिमाइज़र उस गोल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वह कपड़े देखने में और उनके बारे में जानने में कई घंटे बिता देते हैं। अगर एक मैक्सिमाइज़र अपनी खरीदी हुई चीज़ से संतुष्ट ना हो तो भी यह कोई हैरानी की बात नहीं है। एक बार फिर से बता दें कि कई सारे ऑप्शंस में से चुनने में लगने वाली मेहनत की वजह से शॉपिंग करने का मज़ा कम हो जाता है।
मैक्सिमाइज़र का उल्टा होता है सेटिस्फाइसर। सेटिस्फाइसर अपनी पसंद की हुई अच्छी चीज़ से संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे, मान लीजिए की जूलिया एक सेटिस्फाइसर हैं। वह एक स्वेटर खरीदती हैं जो उनके बजट में है और उन पर अच्छा लग रहा है। सेटिस्फाइसर अपनी चॉइस से तब तक खुश और संतुष्ट रहते हैं जब तक वह उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है
ऐसा कहने का मतलब यह नहीं है की सेटिस्फाइसर एवरेज चीजों को पसंद कर लेते हैं। सेटिस्फाइसर के भी अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं पर उन्हें पता होता है की “यह चीज़ मेरे लिए काफी अच्छा है” ऐसा कब कहना है। वहीं, मैक्सिमाइज़र हमेशा दूसरे ऑप्शंस को देखते रहते हैं और चाहते हैं कि उनके पास सबसे बेस्ट चीज़ें हों।
ये हर इंसान पर डिपेंड करता है कि वो मैक्सिमाइज़र है या सेटिस्फाइसर। लेकिन सभी को मैक्सिमाइज़र होने के नुकसान के बारे में पता होना चाहिए। कई सारे ऑप्शन पर ध्यान देने की वजह से आप एंजाइटी या डिप्रेशन महसूस कर सकते हैं। इससे आपको हमेशा पछतावा या अफ़सोस करने की भी आदत हो जाएगी।
क्या इसका मतलब यह है की सेटिस्फाइसर के मुकाबले मैक्सिमाइज़र कम खुश रहते हैं? बैरी श्वार्ट्ज और उनके कलीग्स ने इस थ्योरी को टेस्ट करने का फैसला किया था। इसके लिए पहले उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को एक सर्वे पूरा करने के लिए कहा। इस सर्वे से पता चला की वह मैक्सिमाइज़र हैं या सेटिस्फाइसर।
जिन लोगों का बिहेवियर और एटीट्यूड मैक्सिमाइज़र की तरह बहुत ज़्यादा था उनसे और भी कई सवाल पूछे गए। इन सवालों की मदद से उनकी खुशी और optimism यानी आशावादी होने की quality को नापने की कोशिश की गई। इससे बैरी और उनके कलीग्स को पता चला की जिन लोगों का हाई मैक्सिमाइज़र स्कोर था वे आमतौर पर अपनी ज़िंदगी से कम खुश थे। वो optimistic भी कम थे यानी उनके मन में आशा भी कम थी।
इसका मतलब यह नहीं है की मैक्सिमाइज़र होने की वजह लोग खुश नहीं रहते हैं बल्कि ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे से मज़बूती से जुड़े हुए हैं। अगर आप मैक्सिमाइज़र हैं तो इस बात का बहुत चांस है की आप नाखुश रहेंगे। हालांकि, आप अपनी आदत को बदल सकते हैं और इसके बजाय एक सेटिस्फाइसर बन सकते हैं।
Choice and Happiness
किसी चीज़ को चुनने की आज़ादी होने से हम अच्छे से रह पाते हैं यानी ज़्यादा ख़ुश और हेल्दी रहते हैं। चॉइस से हमें दो वैल्यूज़ मिलते हैं: इंट्रूमेंटल और एक्सप्रेसिव वैल्यू।
इंस्ट्रुमेंटल वैल्यू को मैरियल के रोज़ की ज़िंदगी में देखा जा सकता है। इंस्ट्रुमेंटल वैल्यू होने का मतलब है की मैरियल को ज़िंदगी में जिस भी चीज़ की जरूरत थी या जो भी उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिल जाता था। उनकी ज़िंदगी इसलिए अच्छी थी क्योंकि अपने समय का क्या करना है इसका चुनाव वह खुद करती थी। जैसे मान लीजिए कि मैरियल फैसला करती हैं की वह अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज़, मेडिटेशन और हेल्दी लाइफस्टाइल को शामिल करेंगी। साथ ही वह वेजिटेरियन बनने का भी फैसला करती हैं।
अब, मैरियल की लाइफस्टाइल सबको सूट नहीं करेगी पर ये भी बिल्कुल ठीक है। दूसरे लोग भी, जो उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छे से सूट करता है, उसे choose करके इंस्ट्रुमेंटल वैल्यू पा सकते हैं।
दूसरी ओर, एक्सप्रेसिव वैल्यू उन चीज़ों को चुनने से मिलता है जो दुनिया को यह बताते हैं की हम कौन हैं और हम किस चीज़ की परवाह करते हैं। इस वैल्यू को आपके कपड़े पहनने के ढंग और आपके बर्ताव में देखा जा सकता है। अगर आप बोल्ड कपडे पहनने का फैसला करते हैं तो इसका मतलब हो सकता है की दूसरे क्या सोचते हैं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सप्रेसिव वैल्यू को आपकी हॉबीज़ में, आपके चुने हुए करियर में और भी कई चीज़ों में देखा जा सकता है।
किसी चीज़ को अपनी मर्ज़ी से चुन पाने में सिर्फ़ आपकी आज़ादी शामिल नहीं होती है। यह हमारे साइकोलॉजिकल हेल्थ पर भी असर करता है। इमेजिन कीजिए की आपके चुने हुए चॉइसेस का कोई असर ही न हो तो क्या होगा। जैसे, मान लीजिए की आप एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं पर चाहे आप कुछ भी कर लें आप कोई न कोई गलत चीज़ कर ही देते हैं और इसलिए आप हार मान लेते हैं। इसे ‘लर्न्ड हेल्पलेसनेस’ कहा जाता है (सीखी हुई लाचारी)।
लर्न्ड हेल्पलेसनेस के बारे में साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिगमैन और उनके कलीग्स के एक्सपेरिमेंट्स से पता चला है। उनके एक्सपेरिमेंट में जानवरों के तीन ग्रुप बनाए गए थे। सभी जानवरों को एक रुकावट पर से कूदने के लिए कहा गया ताकि वे बिजली के झटके से बच सकें।
पहले और दूसरे ग्रुप ने धीरे -धीरे सीख लिया की बिजली के झटके से कैसे बचना है। लेकिन, तीसरे ग्रुप की कंडीशन अलग थी। भले ही वह उन रुकावटों के ऊपर से कूद जाते थे पर फिर भी उन्हें झटका लगता था।
अंत में तीसरे ग्रुप के जानवरों ने धीरे-धीरे हार मान ली। वह कूदने के बाद वहीं पर लेट जाते थे और लगातार झटका लगने के बाद भी वहां से हिलते तक नहीं थे। यहीं से लर्न्ड हेल्पलेसनेस के बारे में पता चला। भले ही वह जानवर कुछ भी क्यों न कर लें पर उनके साथ हमेशा वही होता था तो उन्होंने उसके बाद कुछ करने की कोशिश ही नहीं की।
मान लीजिए की आपको भी उस तीसरे ग्रुप के बेचारे जानवरों के जैसा रिजल्ट मिलता रहे यो क्या होगा। कई स्टडीज में इंसान पर बार-बार लर्न्ड हेल्पलेसनेस के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। इसके रिजल्ट बहुत निराश करने वाले थे। उन लोगों में दोबारा कोशिश करने की सारी मोटिवेशन खत्म हो चुकी थी। उनका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो गया था जिस वजह से उन्हें बीमारी होने का ज़्यादा डर रहता था। कुछ स्ट्डीज में, देखा गया की लर्न्ड हेल्पलेसनेस की वजह से क्लिनिकल डिप्रेशन भी हो सकता है।
असल में, हमारी ज़िंदगी पर हमारा कंट्रोल है यह बात पता होना हमारे सेहत के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन, बहुत सारे चॉइसेस होना भी हमारे लिए बुरा हो सकता है। इस ज़्यादा बोझ होने की फीलिंग से बचा जा सकता है। अपनी चॉइस का इस्तेमाल कब करना है इसके लिए selective रहकर हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हमें इस बात को प्रायोरिटी देनी होगी की हमें कब डिसाइड करना है।
आसान तरीके से समझें तो, हमें इस बात का फैसला लेना होगा की हमें फैसला कब लेना है। कैस सनस्टीन एक लीगल स्कॉलर हैं और एडना उल्मन-मार्गालिट एक प्रोफेसर हैं, उन दोनों ने इसे ‘सेकंड-ऑर्डर डिसीजन’ का नाम दिया। सेकंड-ऑर्डर डिसीजन तीन तरह के होते हैं - रूल्स, प्रिजंप्शंस और स्टैंडर्ड्स।
रूल्स उन्हें कहते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता या जिनसे समझौता नहीं किया जा सकता। फ्लाइट में अपने सीट की बेल्ट बांधना एक रूल है तो आप इसे automatically कर लेते हैं। सीट बेल्ट न बाँधने का ऑप्शन आपके दिमाग में कभी नहीं आता है। रूल्स, एक तरह से automatic डिसिशन होते हैं। इसके लिए आपको ऑप्शन को देखना नहीं पड़ता है।
इसका दूसरा example हो सकता है अपने पार्टनर को धोखा देना। यह आपके लिए एक रूल है की आपको कभी अपने पार्टनर को धोखा नहीं देना चाहिए। इसलिए, आपके दिमाग में कभी ऐसा खयाल नहीं आता है की आपको किसके साथ मिलकर उसे धोखा देना चाहिए।
दूसरा सेकंड-ऑर्डर डिसीजन है प्रिजंप्शंस यानी अनुमान लगाना। रूल्स के मुकाबले प्रिजंप्शंस कम स्ट्रिक्ट होते हैं। आप इसे अपने कंप्यूटर में पहले से की हुई सेटिंग की तरह समझ सकते हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं तो उसमें पहले से कैलीब्री फ़ॉन्ट और साइज़ 11 सेट होता है। अब, आप फ़ॉन्ट और उसके साइज़ को बदल भी सकते हैं पर ज्यादातर आप पहले से सेट की हुई सेटिंग का ही इस्तेमाल करते हैं
अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जाना इसका दूसरा example हो सकता है। आपको वही डिश खाने का मन करता है जो आप अक्सर खाया करते हैं, जैसे फ़िश और चिप्स। इसे आपकी डिफॉल्ट चॉइस की तरह समझा जा सकता है। बेशक, मेन्यू में दूसरे आइटम भी हैं जिनमें से आप कुछ भी चुन सकते हैं लेकिन अगर आपको अपना फेवरेट खाना खाने का मन है तो आप फ़िश और चिप्स ही ऑर्डर करेंगे।
तीसरा सेकंड-ऑर्डर डिसीजन है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इन तीनों में सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। एक स्टैंडर्ड बनाने का मतलब है अपने ऑप्शन को दो हिस्से में बाँटना: इनमें से कुछ ऑप्शन स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं, वहीं दूसरे स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं होते हैं। चीज़ों को आसान बनाने के लिए, हम उन ऑप्शंस में से चुनाव करते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड में फिट होते हैं।
जैसे मान लीजिए की आप किस तरह के रेस्टोरेंट में खाना चाहते हैं इसके लिए आपके कुछ स्टैंडर्ड हैं। आपके स्टैंडर्ड्स कुछ ऐसे हैं की: वह जगह साफ़ होनी चाहिए, आपके घर के नज़दीक होनी चाहिए और आपके बजट में होनी चाहिए। अब मान लीजिए की रेस्टोरेंट A, B और C तीनों की इसमें फ़िट होते हैं और रेस्टोरेंट D, E और F इसमें फ़िट नहीं होते हैं। तो बेशक, अब आप रेस्टोरेंट A, B और C में से किसी एक को चुनेंगे क्योंकि यह आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से फ़िट हैं।
पर आप रेस्टोरेंट A, B और C में से किसी एक को कैसे चुनेंगे? याद रखें की सेटिस्फाइसर और मैक्सिमाइज़र, दो तरह के लोग होते हैं। यह इस बात पर डिपेंड करता है की अब आप सारे ऑप्शन को एनालाइज़ करेंगे और उनमें से आपको जो सबसे अच्छा लगेगा उसे चुनेंगे या फिर जो भी आपको ठीक-ठाक सा लग रहा होगा उसे चुनकर संतुष्ट रहेंगे।
स्टैंडर्ड बनाने का फायदा यह है की आप इसे आसानी से आदत में बदल सकते हैं। जैसे, मान लीजिए की आप रेस्टोरेंट B को चुनते हैं। अगर पहली बार आपको वहां जाकर अच्छा लगता है तो आप वहाँ दोबारा भी जाएँगे और ऐसे आपको हमेशा इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी की किस रेस्टोरेंट को चुनना चाहिए।
इस तरह, रूल्स, प्रिजंप्शन और स्टैंडर्ड का होना डिसीजन लेने को आपके लिए आसान और मैनेजेबल बना देता है।
What To Do About Choice
कुल मिलाकर, पिछले कुछ सालों में हमारे लाइफ की quality पहले से बहुत अच्छी हो गई है। हमें हर चीज़ पहले से बनी-बनाई और आसानी से मिलने लगी है। लगभग हर चीज़ के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलने लगे हैं। लेकिन, इन्हें चुनने में इतनी परेशानी होती है की इस वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है।
इस चीज़ के लिए बैरी सुझाव देते हैं की जब आपको कुछ चुनना हो तो नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें। याद रखें की इन स्टेप्स के लिए कमिटमेंट और डिसिप्लिन की जरूरत है इसलिए आपको पूरी शिद्दत से इन्हें अपनी रूटीन में शामिल करना होगा -
इस बात का फैसला करें की आपको फैसला कब करना है। दूसरे शब्दों में, आपको फैसला करने के लिए कभी-कभी कुछ मौकों को छोड़ना होगा। जब आपको अपने ऑप्शंस में से चुनते वक्त बुरा महसूस हो तो यह एक साइन होता है की आपको उस वक्त कुछ choose नहीं करना चाहिए। यहां एक स्ट्रेटजी बताई गई है जो इस चीज़ को देखने में आपकी मदद करेगी की कभी-कभी किसी चीज़ को choose करना कैसे सिरदर्द बन सकता है।
आपने हाल ही में जितने भी छोटे-बड़े फ़ैसले किए हैं उनकी एक लिस्ट बनाएँ। यह एक टेबल लैंप खरीदना या फिर लंबी छुट्टी पर जाना, कुछ भी हो सकता है। फिर, उस फैसले को करने में आपका कितना समय लगा, आपको कितना रिसर्च करना पड़ा, आपको कितना स्ट्रेस और एंजाइटी हुआ, इसे लिखें।
जैसे मान लीजिए की, टेबल लैंप को खरीदने में आपको दो हफ़्ते लगे। ऑनलाइन अलग-अलग तरह के टेबल लैंप को देखने में आपने हर रोज़ 1 घंटे का समय बिताया। यह आपको याद दिलाने में मदद करता है की कोई फैसला लेने में कितना स्ट्रेस हो सकता है।
यह आपको इस बात को याद रखने में मदद करता है की कभी-कभी जिस स्ट्रेस का आपको सामना करना पड़ता है वो उस फैसले के लायक नहीं होता है।
चूज़र बनें, पिकर नहीं। चूज़र वह इंसान होता है जो इस बात पर ध्यान देता है की वह क्या चीज़ है जो एक फैसले को जरूरी बनाता है। एक चूज़र इस बारे में सोचता है की वह ऑप्शन अच्छे हैं या फिर दूसरे ऑप्शन पर ध्यान की जरूरत है। वहीं, पिकर वह इंसान होता है जो कुछ भी अवेलेबल होता है उसमें से ही सिलेक्ट कर लेता है।
पिकर बनने से बचने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा -
पहला, जो फ़ैसला जरूरी नहीं है उनमें लगने वाले समय को कम करें। आपको एक सीरियल ब्रेड को चुनने में 20 मिनट लगाने की जरूरत नहीं है।
दूसरा, इस बात को समझें की आपकी ज़िंदगी में वह कौन से एरिया हैं जहां आपके फैसले सच में मायने रखते हैं। एक सीरियल को चुनना, करियर को चुनने का फैसला लेने के मुकाबले इतना जरूरी नहीं है। इसलिए चीजों को सही तरह से प्रायोरिटी देना ज़रूरी है।
ज़्यादा सेटिस्फाइसर बनें और मैक्सिमाइज़र कम बनें। अगर आप एक मैक्सिमाइज़र हैं तो सेटिस्फाइसर के लिए जो चीज़ें “ठीक-ठाक अच्छी हैं” उनमें संतुष्ट हो जाने के माइंडसेट को अपनाना शुरू करें। याद रखें की सेटिस्फाइसर एवरेज चीज़ें नहीं चुनते हैं या अपने मन को मारकर कोई चीज़ choose नहीं करते हैं, उन्हें बस अपने स्टैंडर्ड का पता होता है और वह कोई चुनने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं।
अगर आप एक सेटिस्फाइसर बनना चाहते हैं तो एक आदत है जिसे आप अपना सकते हैं। अपने लाइफ के किसी ऐसे सिचुएशन के बारे में सोचिए जहां आप comfortably उस चीज़ को चुन सकते हैं “जो आपके लिए अच्छी” हो। हो सकता है की इसका मतलब फ़ोन A और C के बजाय फ़ोन B को खरीदना हो क्योंकि फ़ोन B आपके लिए ठीक-ठाक अच्छा है। फिर, आप फ़ोन के लिए इस्तेमाल किए गए सेम थिंकिंग पैटर्न को अपने ज़िंदगी के दूसरे एरिया में भी अप्लाई कर सकते हैं।
अपने फ़ैसले को non-reversible यानी ऐसा बनाएँ की उन्हें बदला नहीं जा सकता हो। लगभग हर इंसान किसी ऐसी दुकान को चुनता है जहां पर चीज़ें return की जा सकती हों पर अपना मन बदल पाने की आज़ादी होने से आपको बस अपने चॉइस को लेकर स्ट्रेस और अफ़सोस होता रहेगा।
इसलिए, ऐसे फैसले लें जिन्हें बदला नहीं जा सकता हो। ऐसे फैसले लेने से आपको दूसरे अवेलेबल ऑप्शन के बारे में कम सोचने में मदद मिलती है।
Example के लिए, एक रिलेशनशिप में होने का मतलब है सिर्फ़ एक इंसान के लिए कमिटेड रहना। अगर आप इस बारे में सोचने लगेंगे की कैसे दूसरे लड़के और भी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं तो आपको उनके पीछे जाने का मन करेगा। इस सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं की अभी जो आपका पार्टनर है उस पर और आप अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं इस बात पर ध्यान दें। “अगर वैसा होता तो क्या होता”, इन बातों के बारे में सोचने से बस आपकी परेशानी ही बढ़ेगी और आपके हाथ कुछ नहीं आएगा।
Conclusion
सबसे पहले, आपने जाना की हर चीज़ के लिए आज सभी के पास बहुत सारी चॉइस मौजूद हैं। जैसे फ़ूड प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, स्मार्टफोन, कॉलेज, कोर्सेज, जॉब और ना जाने कितना कुछ। शॉपिंग करने में आजकल लोग पहले से ज़्यादा समय बिताने लगे हैं।
हालांकि, रिसर्च से पता चला है की ज़्यादा ऑप्शन होने से हम खुश नहीं होते हैं। असल में, ज़्यादा चॉइसेस होने की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस में से चुनने में लगनी वाली मेहनत, ज़्यादा ऑप्शन होने की खुशी को खत्म कर देता है।
दूसरा, आपने मैक्सिमाइज़र और सेटिस्फाइसर के बारे में जाना। जो लोग मैक्सिमाइज़र होते हैं वह सभी ऑप्शन को देखते हैं ताकि वह सबसे बेस्ट चीज़ को choose कर पाएँ। वहीं, सेटिस्फाइसर में “जो भी उनके लिए अच्छा है” उसे अपना लेने का माइंडसेट होता है। वह मन मारकर नहीं रहते या एवरेज चीज़ सिलेक्ट नहीं करते हैं बल्कि वह अपने स्टैण्डर्ड के हिसाब से चुनी चीज़ से संतुष्ट रहते हैं।
तीसरा, आपने जाना की हमारी खुशी के लिए चॉइसेस कितने जरूरी होते हैं। हमारी चुनी हुई चीज़ का कोई असर नहीं होने वाला है, ये जानने के बाद लर्न्ड हेल्पलेसनेस हो सकता है। हालांकि, बहुत सारे ऑप्शंस होने की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो सकता है। स्ट्रेस से बचने के लिए, हमें सेकंड-ऑर्डर डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा तब होता है जब आप रूल्स, प्रिजंप्शंस और स्टैंडर्ड्स सेट कर लेते हैं।
आखिर में, आपने जाना की आपको फैसले कैसे लेने चाहिए। याद रखें की आपको इस बात का फैसला लेना है की आपको फैसला कब लेना है. एक चूज़र बनें, पिकर नहीं। सेटिस्फाइसर बनना सीखें और आखिर में ऐसे फैसले लें जिन्हें बदला न जा सकता हो। हर चीज़ पर गहराई से ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। अपनी चॉइस से खुश रहें और जो चीज़ें जरूरी हैं उनके ऊपर ध्यान दें।
एक कहावत है की, “दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है”, जिसका मतलब होता है कि आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। आपकी काबिलियत का कोई अंत नहीं है पर सबसे बेस्ट हासिल कर पाने का सिर्फ़ एक ही तरीका है कि आप समझदारी से choose करें।
राशन के सामान के ब्रैंड के बारे में ज़्यादा न सोचें और अपने फैसले लेने की एनर्जी को ज़िंदगी के दूसरे बड़े डिसिशन के लिए बचाकर रखें, जैसे की आपके करियर और रिलेशनशिप के लिए। जब बात फैसला लेने की आती है तो खुद को लिमिट में रखने से आपको ज़िंदगी में ज़्यादा खुश रहने में, ज़्यादा कामयाब महसूस करने में और ज़्यादा संतुष्ट रहने में मदद मिलेगी।